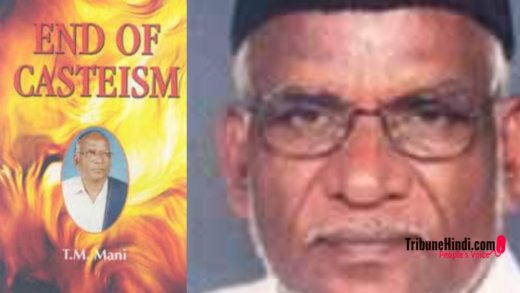जब हम ‘मुल्क’ देख कर बाहर निकले, तो हमारे एक मित्र ने कहा कि ‘मुल्क’ जो बात कहती है, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आज का हिंदुस्तानी मुसलमान कहने की स्थिति में नहीं है। ‘मुल्क’ क्या कहती है? ‘मुल्क’ कहती है कि कोई मुसलमान अपनी देशभक्ति प्रमाणित कैसे करे? क्यों करे? वह ख़ुद पर चस्पां कर दिये गये आतंकवादी कौम के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या करे कि सरकार और हिंदू पड़ोसियों को लगे कि वह भी एक सच्चा भारतीय है? ‘मुल्क’ इन सवालों से निर्भीक होकर टकराती है और इसलिए टकरा पाती है, क्योंकि फ़िल्मकार अनुभव सिन्हा एक हिंदू हैं। मौजूदा सरकार की मातृ-संस्था आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से एक “तथाकथित और भटका हुआ हिंदू”, जिसे अपने धर्म के उत्थान-पतन से ज़्यादा इंसानियत के उत्थान-पतन की चिंता है। मैंने ग़ौर किया कि न सिर्फ़ निर्देशक अनुभव सिन्हा, बल्कि ‘मुल्क’ में एक भी कलाकार मुसलमान नहीं है। चूंकि मैं अनुभव से पूछ सकता हूं, इसलिए मैंने पूछा तो उन्होंने बिना किसी संकोच के यह जवाब दिया कि हां, यह एक सचेत कोशिश थी – क्योंकि ‘मुल्क’ जो बात कहती है, वह आज किसी भी मुसलमान से ज़्यादा हिंदुओं को कहने की ज़रूरत है।
अनुभव सिन्हा ऐसे फ़िल्मकार रहे हैं, जिन्होंने आज तक एक भी राजनीतिक फ़िल्म नहीं बनायी थी। ‘तुम बिन’ से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले अनुभव सिन्हा की फ़िल्मों का विषय रहा है, रोमांस, अपराध, सस्पेंस, थ्रिलर, साइंस फ़िक्शन वगैरा-वगैरा। सात बड़ी फ़िल्में बनाने के बावजूद उन्हें लगा कि वह फ़िल्मकार नहीं हैं, क्योंकि फ़िल्मकार के पास एक दायित्व भी होता है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उनकी फ़िल्मों में उनका मुल्क, उनका समाज नहीं है। पिछले दिनों भारतीय राजनीति जिस तरह से अपने ही नागरिकों में फर्क करते हुए विद्वेष की बिसात बिछाने में दिलचस्पी लेने लगी, उनके निर्देशक मन ने अपनी शैली से यू-टर्न लेने की ठान ली। इस लिहाज़ से ‘मुल्क’ आज के समय की प्रतिनिधि फ़िल्म है, जो यह कहती है कि अच्छे और बुरे लोग हर कौम में समान मात्रा में होते हैं। इसलिए कुछ बुरे लोगों की वजह से हम एक कौम को नहीं घेर सकते और उनके लिए घेटो बनाने की तरफ़ नहीं बढ़ सकते। इसके लिए ‘मुल्क’ बहुत ही आसान टूल हमें थमाती है कि इतिहास को हम वॉट्सएप और फेसबुक-ट्विटर के ज़रिये न समझें बल्कि इसके लिए विश्वसनीय किताबों की गली में जाएं। मंदिर में भाषण देना बंद करें और संसद में पूजा से बाज आएं।
अनुभव सिन्हा की फ़िल्म यह भी बताती है कि मुल्क आज जो है, उसकी नींव ही छुआछूत और सामाजिक वैमनस्यता से भरी हुई है। यही वजह है कि धार्मिक एजेंडे वाली राजनीतिक पार्टियों को मुल्क के भीतर मुल्क के तथाकथित दुश्मनों की पहचान करने में आसानी हो जाती है। हमें बचपन से कुछ चीज़ें बतायी गयी हैं, जिसके चलते मिथ की तरह हम मानने लग जाते हैं कि मुसलमान गंदे होते हैं, उनके साथ अलग बर्तन का बर्ताव रखना चाहिए, वे एक से ज़्यादा शादियां करते हैं और बेशुमार बच्चे पैदा करते हैं, पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़ते हैं, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है और मस्जिदों में हिंसक जिहाद की रणनीति बनती है – आदि आदि। ये बातें चूंकि बचपन से हमारे दिमाग़ पर हावी रहती हैं, इसलिए इससे निकल पाना आसान नहीं होता। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हम मुस्लिम मोहल्लों में जाने से परहेज़ करते हैं और मुस्लिम दोस्त बनाने से भी। ठीक ऐसी ही समझदारी दलितों के बारे में हमारे भीतर डाली जाती है। ‘मुल्क’ बताती है कि इस ग़लतफ़हमी को हवा देना भी आतंकवाद है और ग़रीब-निर्दोष दलितों और आदिवासियों की हत्या करना भी आतंकवाद है।
‘मुल्क’ बनारस के एक मोहल्ले की कहानी है, जिसमें हिंदू आबादी भी है और मुसलमान आबादी भी। आपसी भाईचारे में वह राजनीतिक नारा सेंध लगाता है, जो चीख़ कर कहता है कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हैं। हिंदू हम हैं और मुसलमान वे हैं। भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है और मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसलिए जब एक परिवार का नौजवान आतंकवादी बन जाता है, तो उसकी दीवार पर रात के अंधेरे में नारा लिख दिया जाता है कि पाकिस्तान जाओ। फ़िल्म यह सवाल करती है कि अगर हिंदू परिवार का आतंकवादी होता, तो क्या उसकी दीवार पर भी यही नारा लिखा जाता? हालांकि इसका जवाब भी आजकल के पेड ट्रोलर्स देते रहते हैं कि ‘सेकुलर हिंदुओं’ को भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जैसे अगर आप सच्चे हिंदू हैं, तो स्वाभाविक तौर आपको मुसलमानों के प्रति नफ़रत से भरा होना चाहिए। ‘मुल्क’ सच्चे हिंदू होने का अर्थ समझाने की कोशिश करती है। अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं में आस्था रखते हुए एक-दूसरे के साथ रहने और आपसी मोहब्बत की पटरी से न उतरने की वकालत करती है।
जब तक मैंने ‘मुल्क’ नहीं देखी थी, मुझे हैरानी हो रही थी कि सेंसर बोर्ड ने ऐसी फ़िल्म को प्रमाणपत्र कैसे दे दिया जो आज के राजनीतिक माहौल में सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे की हवा निकाल रही हो। लेकिन जब मैंने फ़िल्म देखी, तो मुझे लगा कि इसमें तर्क का ऐसा मज़बूत महल खड़ा किया गया है, जिसे अफ़वाहों के तेज़ हथौड़ों से भी तोड़ा नहीं जा सकता। आख़िर में फ़िल्म का खलपात्र कहता भी है कि आज फ़िर न्याय ने धर्म को चित्त कर दिया। ‘मुल्क’ एक तार्किक फ़िल्म है और सेंसर बोर्ड के लिए उन तर्कों पर कैंची चलाना लगभग असंभव था। अगर यह भावुक फ़िल्म होती, तो फिर इसे सरकार प्रायोजित सेंसर के सामने ख़ुद को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता। एमएस सथ्यू की ‘गरम हवा’ के बाद ‘मुल्क’ ही वह फ़िल्म है, जो हिंदू-मुस्लिम के सामाजिक ताने-बाने को क़ायदे से समझती हुई दिखती है। उन देशों में भी साहसिक और प्रतिरोधपूर्ण राजनीतिक फ़िल्में बनाने की परंपरा है, जो भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश नहीं हैं। लेकिन भारत में ही ऐसी फ़िल्मों की कमी है। इस सदी में ‘मुल्क’ से एक बेहतर शुरुआत हुई है। अनुभव सिन्हा और उनकी पूरी टीम को बधाई।